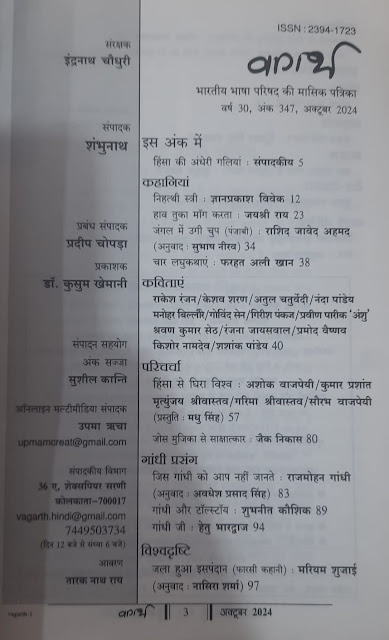उस दिन वे मिले तो मधु घोलते हुए।
तपाक से हाथ मिलाया, हाल-चाल पूछा, घर-गृहस्थी की चर्चा की। मैंने सोचा, चलो कोई तो आत्मीयता दिखाने वाला मिला। नई जगह पर परिचित व्यक्ति जरूरी होता है।
जब मैंने डिपार्टमेंट में प्रवेश किया तो किसी तेज तंबाकू की सुगंध मेरे नथुनों में जबरदस्ती घुसने की जिद करने लगी। मेरी निगाह उसी ओर घूम गई।
पतली मोरी की पैंट पर खद्दर की कमीज धारण किए हुए एक महाशय बनारसी स्टाइल में बीड़ा चबा रहे थे। लगता था कि इसके साथ ही वे सारे परिवेश को पीने की ख़ास कोशिश कर रहे थे।
नमस्कार-निवेदन के बाद मैंने अपना परिचय दिया तो वे चहक उठे,‘वाह, वाह आप ही हैं। आइए-आइए, बैठिए-बैठिए। बड़ी ख़ुशी हुई आपके आने पर। एक साथी बढ़ गया।’
उनके वार्तालाप से ही पता चल गया कि वे भी यहीं की तोड़ रहे हैं और मुझसे सीनियर है।
मैं नतमस्तक हो गया।
बोले,‘कोई परेशानी हो तो बताइएगा। मैं आपके किस काम आ सकता हूँ?’और इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय के संपूर्ण भूगोल, समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र पर सेवापूर्व दीक्षा-भाषण दे डाला। दीक्षांत भाषण तो मैंने डिग्री लेते हुए कई बार अनमने मन से सुने थे, किंतु इस भाषण को पता नहीं क्यों, ध्यानपूर्वक सुनता रहा।
दीक्षांत समारोह के विशाल पंडाल में जगमगाती हुई रोशनी से दिया जाने वाला औपचारिक भाषण मुझे सदैव उबाता रहा है। वही औपचारिक शपथ बी॰ए॰ से लेकर पी-एच॰डी॰ की डिग्री तक बार-बार दुहराता रहा और फिर सम्मानित मुख्य अतिथि का लिखा भाषण, जिसकी छपी प्रतियाँ पहले भी बँट जाती थीं, बड़ा बोर करता था। लगता था कि इसका जीवन से कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है और प्रायः मैं पंडाल में औपचारिकता निभाने के ख़याल से ही बैठा रहता था, अन्यथा मन तो भविष्य के सपने सजाने में सोने की तैयारी में लगा रहता था।
किंतु पता नहीं इस भाषण में क्या आकर्षण था कि मंत्रमुग्ध-सा सुनता रहा। अब मैं धनुषाकार हो गया था। यदि वहाँ जगह होती तो साष्टांग करने की इच्छा पूरी कर लेता। इतने में ही किसी दूसरे विभाग के प्राध्यापक भी वहाँ आ गए थे। इसलिए यह अवसर मेरे हाथ से निकल गया। तभी मन ने कहा-‘अच्छा ही हुआ। पहली भेंट में इतना ही काफ़ी है।’
वे दोनों काफ़ी देर तक विद्यालय का भूगोल डिस्कस करते रहे। समाजशास्त्र में चलती हुई गाड़ी राजनीति के स्टेशन पर आकर सीटी देने लगी। अभी तक मैं निस्पृह भाव से आगे की सोच रहा था, किंतु अब मेरे कान भी खड़े हो गए। मैंने पहली बार समझा कि भूगोल और समाज से बचकर निकला जा सकता है, किंतु राजनीति के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं और इनमें भारी पावर का चुंबक भी लगा है। ये हमारे तन-मन को अपनी ओर खींचकर एकदम बंद हो जाते हैं। बचो बच्चू! कैसे बचोगे?
मुझे एहसास हुआ कि नुक्कड़वाले की चाय की दुकान से लेकर कालेज की कैंटीन तक सभी राजनीतिज्ञ हैं। जो इससे अलग है, वह संसार का सबसे व्यर्थ व्यक्ति है। अपने अस्तित्व के लिए किसी के साथ जुड़ना और किसी से कटना जरूरी है। बीच में नहीं रह सकते। होता होगा मध्यम मार्ग। चलते होंगे साधक उन पर भी, किंतु अब तो राजनीति की मोटर आपको घायल करती हुई निकल जाएगी। फिर तो पोस्टमार्टम के लिए भी पुलिस ही उठाएगी। भीड़ तो अपने रास्ते निकल जाती है।
मन में कैसी-कैसी कड़वाहट भर गई। मैं बड़ी घुटन-सी महसूस कर रहा था। पंखे की खर्र-खर्र में भी मेरी साँस मुझे साफ़ सुनाई दे रही थी। मुझसे वहाँ न रुका गया। मैं वहाँ से उठ आया।
एक सप्ताह बीत गया। एक कहावत है-नया मुल्ला अल्ला-अल्ला पुकारता है। मैं छात्रों पर अपना प्रथम प्रभाव डालने में व्यस्त था। पता नहीं छात्रों को एक ही बार पंडित बनाने का भूत क्यों सवार हुआ?(अब तो मैं स्वयं भूत बन चुका हूँ) मुझे इस बात का भी ध्यान न रहा कि विद्यालय में प्राचार्य नाम का भी जीव रहता है और कभी-कभी उसके दर्शन करने अनिवार्य हैं। भगवान की एक क्वालिटी के विषय में मैं सदैव से आश्वस्त रहा हूँ कि तुम उसे भले ही याद न करो, वह तुम्हें अवश्य याद कर लेता है।
लायब्रेरी के एक कोने में कुर्सी पर आसीन मुझको किसी की आवाज ने चौंका दिया। गर्दन उठाई तो मेरे सामने चपरासी रूपी देवदूत (यमदूत भी कह सकते हैं।) एक कागज लिए हुए खड़ा था। अबू बेन ऐदम के समान मैं उससे उस लिस्ट के विषय में पूछने ही वाला था कि ‘हे देवदूत, इस पर किनके नाम लिखे हैं? क्या तुम भी अच्छे आदमियों के नाम नोट कर रहे हो?’ पर कुछ सोचकर रुक गया।
उसने अपनी स्वाभाविक वक्रता के साथ पूछा,‘आप ही अग्रवाल साब हैं?’ कहना तो चाहता था कि मिस्टर, तुम्हें बंदर या लंगूर दिखाई दे रहा हूँ? किंतु अपने चेहरे का ख़याल करके चुप रह गया। फिर इस चपरासी नामक जाति का बहुत नहीं तो थोड़ा-बहुत अनुभव अवश्य है, यह विशिष्ट प्राणी अपने को सबका बॉस समझता है।
एक बार की बात है। मैं इंटर में पढ़ता था। जाड़ों के दिन थे। प्रधानाचार्य महोदय धूप में बैठे चारों ओर का निरीक्षण कर रहे थे। वे अपने पास दूसरी कुर्सी रखना अपना अपमान समझते थे। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति उनके पास आकर खड़े-खड़े बात करे। चांस की बात, उनका साला विद्यालय में ही चला आया। उन्होंने चपरासी को कुर्सी लाने के लिए आवाज लगाई। मंगू ने खचेडू को खचेडू ने कूड़ेसिंह और कूड़ेसिंह ने कल्लू को कुर्सी लाने का आदेश दिया और शांति के साथ अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे। चारों ओर ‘कुर्सी-कुर्सी’ का शोर मच गया,किंतु कुर्सी न आई।
ऐसा सोचकर मैंने कहा,‘कहिए, क्या काम है?’
‘आपको प्रिंसिपल साब ने याद किया है।’ वह गंभीरता के साथ बोला।
‘कोई विशेष बात है?’ मैंने सवाल किया।
‘उनसे ही पूछिए।’ मानो वह प्रिंसिपल नहीं तो उन जैसा ही कुछ हो।
मुझे याद आया। मैंने अभी तक उनके आफ़िस के द्वार पर सिजदा नहीं किया है। एक फुरहरी-सी मेरे शरीर में दौड़ गई। जैसे किसी ने बर्फ़ का एक टुकड़ा मेरे कॉलर में डाल दिया हो।
प्राचार्य के आफ़िस में पूछकर जाने का रिवाज था। हड़बड़ी में मैं इस रिवाज का ध्यान न रख पाया। छात्रें को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से छूट मिली हुई थी। प्रिंसिपल साहब ने बिना मुँह उठाए पूछा, ‘कहो-कहो, क्या काम है? एप्लीकेशन लाए होगे। लाओ-लाओ।’ मैं मन-ही-मन ख़ुश हुआ कि हमारा प्राचार्य बड़ा दयालु और मिष्टभाषी है।
मैंने कहा,‘सर, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं लाया। आपने---।’
नीचे कागज पर दृष्टि गड़ाए हुए ही उन्होंने कहा,‘क्या, क्या कहा, मैंने क्या?’
‘सर, आपने मुझे बुलाया था। मेरा नाम अग्रवाल। हिंदी विभाग में।’
प्राचार्य की मुखमुद्रा बदली होगी, उस पर सिलवटें भी पड़ी होंगी, मुँह पर कसैलापन भी उभरा होगा, दृष्टि भी वक्र हुई होगी, मुझे नहीं पता। मेरी दृष्टि तो नीचे की ओर थी। मैंने तो केवल इतना ही सुना, ‘ठीक है, ठीक है। किंतु आपको पता है, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। आपको प्राचार्य के पास आने के मैनर्स भी पता नहीं? महोदय, आगे से ध्यान रखिएगा। आप जा सकते हैं।’
मैं सर पर पैर रखकर भागा। मुझे फिर अहसास हुआ कि टुकड़ा डालने वाला रोब दिखाता ही है। चाहे छात्र हो अथवा प्राचार्य। यह अपनी-अपनी शक्ति पर निर्भर है कि हाथ से छीन भी लो और गुर्राओं भी अथवा पूँछ हिलाते हुए तलुवे चाटा करो।
मेरा मुँह एक बार फिर कड़वा हो गया।
पंद्रह दिन बीत गए। कोई हलचल नहीं हुई।
सारा कार्यक्रम बख़ैरियत चलता रहा। कभी-कभी अपने सीनियर मित्र से सलाह-मशवरा लेना अपना धर्म समझता था। उनकी वरीयता इस बात की डिमांड भी करती थी कि मैं बार-बार अपने जूनियर होने का भरोसा दिलाता रहूँ। मन को यह कहकर दिलासा दिलाता-‘फिक्र न करो, तुम्हारा क्या जाता है। चुप रहो, बोलना और मुँह खोलना अपने पाँव में ख़ुद कुल्हाड़ी मारना है।’ दिल ही तो था, कोई छात्र तो नहीं, इस नाजायज दबाव को मान लेता।
क्लासरूम में घुसा और हाजिरी रजिस्टर की पूँछ काटनी शुरू की। कितना उबाऊ काम है हाजिरी लेना। पचास सिंह और पच्चीस पुरुषवाचक रानियों की सूची का हनुमान चालीसा रोज पढ़ना पड़ता है। इस छात्र-स्वतंत्रता के युग में जेलर की हाजिरी परेड का औचित्य ही क्या है?‘न आने वालों’ को कौन बुला सकता है और जानेवालों को कौन रोक सकता है? है किसी में हिम्मत उनको परीक्षा में बैठने से रोक सके। इतना सोचते-सोचते रजिस्टर बंद कर दिया। आखि़री नाम जो आ गया था।
व्याकरण भी क्या बला है? छात्रों के सिर पर तलवार-सी लटकती रहती है। दुर्भाग्य से मैं इसकी राह का राहगीर बना दिया गया हूँ। मेरा वश चलता तो अपनी टाँग तोड़े पड़ा रहता। वह तो भविष्य का ख़्याल करके चुप रह जाता हूँ।
मेरे खड़े होते ही एक छात्र ने सवाल किया,‘सर आपने कहा था ‘निर’ उपसर्ग जिस शब्द में लग जाता है, उसका अर्थ निषेधात्मक हो जाता है जैसे निर्दोष, जिसमें दोष न हो, निर्बल जिसमें बल न हो, निरंकुश जिस पर अंकुश न हो।’
बात ठीक थी माननी पड़ी।
फिर सर,‘निर्माता’ का अर्थ क्या हुआ?
मेरे बोलने से पहले ही एक दूसरा छात्र बोल पड़ा,‘जिसके माता न हो, सर।’
क्लासरूम में हँसी का बम बिस्फोट हो चुका था और मैं घुग्घू की भाँति सबको टाप रहा था। सारी व्याकरण धरी रह गई। लगा सैकड़ों गधे एक साथ मेरे कानों पर रेंक रहे हों।
विषय से हटकर मैं समाज की चर्चा करने लगा। मुझे सबके भविष्य की चिता एक साथ सताने लगी। देर तक उनकी सफलता के गुर बताता रहा। परीक्षा से फैलती-फैलती दीक्षा-गाथा जीवन और जगत् तक पहुँच गई।
मुझे एक अहसास हुआ कि असफलता व्यक्ति को दार्शनिक बना देती है और मैं दुनिया-भर के दार्शनिकों की जीवन-कथाओं को दोहराने लगा था।
✍️ डॉ गिरिराज शरण अग्रवाल
ए 402, पार्क व्यू सिटी 2
सोहना रोड, गुरुग्राम
78380 90732